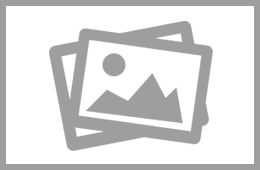राजा और रानी ......!
मानसूनी की पहली फुहारे जब धरती पर पड़ती है तो इंसानों के साथ साथ कीट पंतगे भी बेहद खुशी से झुम उठते है। हर जगह नये नये कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ते है। अक्सर पहली बरसात के बाद से खेतों एवं रेतीली जमीन पर लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े घुमते हुये नजर आते है।
लाल रंग की मलमल ओढ़े ये कीड़े बहुत ही सुंदर लगते है। यहां बस्तर में इन्हे रानी कीड़ा कहते है। रानी कीड़ा मतलब ही किसी रानी की तरह बेहद ही सुंदर। यह कीड़ा रेड वेल्वेट माईट है। इसके पीठ की त्वचा बिल्कुल मलमल की तरह मुलायम होती है।
बच्चे तो इन कीड़ो से बड़ा प्रेम करते है। जब भी ये दिखते है बच्चे इन्हे तुरंत उठा लेते है। हथेली में लेते ही ये अपने सभी पैरों को सिकोड़कर निष्क्रिय हो जाते है। जमीन पर छोड़ते ही भाग जाते है। आप में से प्रायः सभी ने इन रानी कीड़ो को देखा होगा।
मैं इसे कई सालों से देख रहा हूं। दो दिन पहले मैने राजा और रानी दोनो को खेत की मेड़ पर घुमते हुये देखा तब मैंने राजा और रानी दोनो को अपने हथेली पर ले लिया, रानी तो मुझसे नाराज हो गई, बिल्कुल कैकेयी की तरह कोप भवन में चली गई थी। राजा साहब बहुत ही मचलने लग गये थे, तुफान मचा दिया था मेरे हाथ पर, फिर मैने उन्हे उसी जगह छोड़ दिया जहां से उन्हे उठाया था।
ये कीड़े पुरे देश में पाये जाते है, इस कीड़े से बहुत रोगों की दवा भी बनती है जिसके कारण ये कीड़े अब दिखाई नहीं देते है। मधुमेह, लकवा आदि के लिये इसे असरकारक दवा बनायी जाती है। कई क्षेत्रो में ग्रामीण इसे एकत्र करके बेचते है।
आपने भी बचपन में यह रानी कीड़ा देखा होगा, अलग अलग क्षेत्रो में यह कई नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते है ? अपना अनुभव जरूर शेयर करे। ...........ओम.!