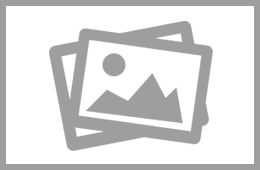बस्तर का 1842 का तारापुर विद्रोह.....!
सत्ता के लालच मे दरियादेव ने बस्तर को अंग्रेजी और मराठा शासन के अधीन कर दिया. अप्रैल 1778 इस्वी की कोटपाड़ सन्धि ने मराठा और अंग्रेजो को बस्तर मे प्रवेश सुगम कर दिया. कोटपाड़ की सन्धि के एवज मे दरियादेव कम्पनी सरकार, मराठो एवं जैपुर राज्य की मदद से अपने भाई अजमेर सिंह को पराजित करने मे सफल हो पाया.
इस सन्धि के बदले जहाँ धाराधिनाथ दरियादेव बस्तर के सिंहासन पर बैठने मे सफल रहा वही बस्तर के महत्वपूर्ण परगने जैपुर राज्य मे चले गये. नागपुर के भोसलो को सालाना टकोली देने की शर्त भी स्वीकार करनी पडी. अंग्रेज तो बस बस्तर मे प्रवेश के मौके का इंतजार कर रहे थे, कोटपाड़ सन्धि से उन्हे यह अवसर आसानी से मिल गया. आंग्ल मराठा शासन के नियंत्रण का नुकसान सबसे अधिक बस्तर की रियाया को उठाना पडा. आंग्ल मराठो के अनुचित हस्तक्षेप से बस्तर की जनता को विद्रोह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा.
फिर तो विद्रोह का सिलसिला चल पडा. 1825 इस्वी के परलकोट के विद्रोह से प्रारम्भ हुआ यह सिलसिला 1910 इस्वी के भूमकाल विद्रोह तक चलता रहा.1842 इस्वी का तारापुर विद्रोह भी मराठा अतिक्रमण और राजपरिवार मे मराठो एवं अंग्रेजो के अनुचित हस्तक्षेप से उपजा हुआ विद्रोह था.1818 इस्वी की आंग्ल और भोसलो की सन्धि से बस्तर की शक्तियां सीमित कर दी गयी. इस सन्धि से भोसले राजा बन गये और राजा जमीदार बन गये. संधि फलस्वरुप बस्तर से वसूली जाने वाली टकोली मे भी बढोतरी की गयी. जिसका परिणाम स्वरुप तारापुर में विद्रोह हुआ.दरियादेव की मृत्यु के बाद 1800 इस्वी मे दरियादेव का पुत्र महिपाल देव बस्तर के राजा बने. महिपाल देव के तीन पुत्र हुए भूपालदेव, दलगंजन सिंह और निरंजन सिंह. महिपाल देव की मृत्यु के बाद 1842 इस्वी मे भूपाल देव बस्तर के राजा बने. भूपालदेव ने अपने भाई लाल दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बना दिया. लाल दलगंजन सिंह दबंग व्यक्तित्व, सदाचारी एवं पराक्रमी था. वह अपने सदव्यवहार से बस्तर की जनता मे अधिक लोकप्रिय था. भूपालदेव और दलगंजन सिंह मे अनेक कारणो से अनमेल रहा.जगदलपुर से 26 किलोमीटर की दुरी पर अवस्थित तारापुर परगना रियासत काल मे राजस्व श्रोत के बजाय जैपुर राज्य के विरुद्ध सैनिक छावनी के रुप मे माना जाता था. तब गर्वनर के रुप मे लाल दलगंजन सिंह तारापुर परगने की देख रेख कर रहे थे.बस्तर राजा ने नागपुर सरकार के आदेश पर तारापुर परगने की टकोली बढा दी थी तब तारापुर के गवर्नर लाल दलगंजन सिंह ने विरोध किया. जब दलगंजन सिंह पर नागपुर सरकार का दबाव बढा तब तो उन्होने टकोली के माध्यम से लूट की स्वीकृति के बजाय तारापुर छोड़ देना का निश्चय किया. तारापुर के आदिवासियो ने लाल को तारापुर छोड़ कर ना जाने का आग्रह किया और लाल दलगंजन सिंह के नेतृत्व मे आंग्ल मराठा शासन के विरुद्ध बगावत करने का निर्णय किया.तारापुर विद्रोह के और भी कारण थे जैसे मराठो की रसदपूर्ति मे सहायक बंजारो ने आदिम जीवन शैली को भंग कर दिया था. तारापुर पर परगने पर राजस्व की माँग बढ़ने के कारण निरन्तर अवैधानिक टैक्स वसूले जा रहे थे और रैय्यत उससे परेशान हो चुकी थी. लाल दलगंजन सिंह और उसके साथी, दीवान जगबन्धु के द्वारा नित्य प्रति नये टैक्स के आरोपित करने के कारण बहुत उत्तेजित थे और उनकी माँग थी कि जब तक दीवान जगबन्धु को हटा नहीं दिया जाता और सारे टैक्स वापस नहीं ले लिये जाते, आदिवासी संघर्ष करते रहेगे.आदिवासियो ने एक दिन दीवान को पकड़ लिया और उसे अपने नेता दलगंजन सिंह के सामने तारापुर में प्रस्तुत किया तब राजा भूपालदेव ने जगन्नाथ बहीदार के हाथो सन्देश भेजा कि दीवान को मुक्त किया जाया. दलगंजन सिंह को आदिवासियो के भारी विरोध के बावजूद भी दीवान को मुक्त करना पड़ा.रिहा होने के बाद दीवान जगबन्धु भूपालदेव के आदेश से नागपुर गये. वहां उन्होंने नागपुर के अधिकारियो से तारापुर विद्रोह को कुचल देने की सहायता मांगी. नागपुर की सेनाओ ने बस्तर कूच किया. तारापुर मे आदिवासियो के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ. विद्रोही सेना पराजित हुई. दलगंजन सिंह को नागपुर की सेनाओ के समक्ष आत्म समर्पण करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर ले जाया गया जहाँ उन्हे छ महिने की जेल हुई. आदिवासियो के असंतोष को दुर करने के लिए नागपुर के रेजीडेण्ट मेजर विलियम्स ने बाद मे जगबन्धु को दीवान के पद से हटा दिया और तब विद्रोह शान्त हो गया, क्योकि वैसी स्थिति मे सारे नये अध्यारोपित टैक्सो को वापस ले लिया गया था.
आलेख - ओमप्रकाश सोनी
संदर्भ..1 बस्तर का मुक्ति संग्राम - शुक्ल हीरालाल
2 बस्तर भूषण - केदारनाथ ठाकुर
3 बस्तर इतिहास और संस्कृति - लाला जगदलपुरी
आप बस्तरभूषण को instagram मे @bastar_bhushan फ़ालो कर सकते हैं.